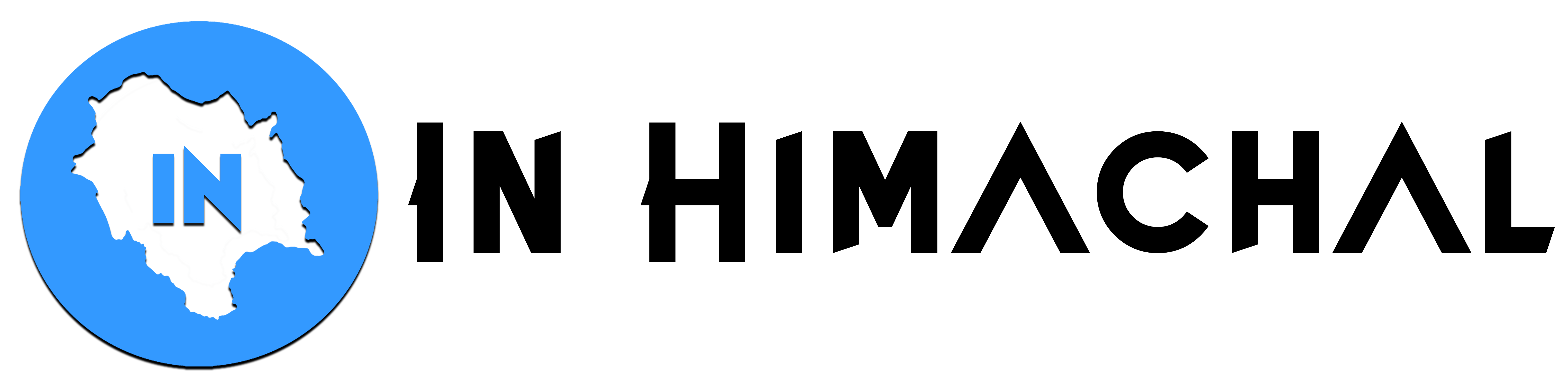दीपक शर्मा।। ठेठ पहाड़ी घरों में मेहमानों को सीधे ड्राइंग रूमों में नहीं हांका जाता। पहला स्वागत रसोई में चूल्हे के ताप से ही होता है। फिर गुनगुने पानी से पैर धुलाए जाते हैं। बारहों महीने की सर्दी और मीलों लंबी पहाड़ी पगडंडियों का पैदल सफर; ज़ाहिर है प्रदर्शनीयता पर प्रैक्टिकेलिटी भारी होती है। लंबे हाल-चाल के बाद स्निग्ध आंच में गंवई गॉसिप घंटों सिंकती है।
इसी चूल्हे से मोड़ी (भुने हुए गेहूं के दाने), बिज्या (भांग के बीजों से बना नमक) और राख में दबाकर भूने गए आलू जैसी अनूठी खाने की चीज़ें निकलती रहती हैं जो दुख-सुख, शिकवे-सनेहों के ज़ायके को और भी गाढ़ा कर देती हैं। हमारा राष्ट्रीय पेय चाय तो खैर होती ही है। चूल्हे के ही इर्द-गिर्द खाना लगता है। जब तक लकड़ियां सुलगती हैं, गप्पबाज़ी का सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद कोयलों को अंगीठी में डालकर अपने-अपने बिस्तरों का रुख़ किया जाता है।

अगर आपके बचपन पर किसी पहाड़ी गांव की छाप है तो शायद आपके लिए चूल्हे में जलती चीड़ की लकड़ियों की सौंधी गंध को भुलाना आसान नहीं होगा। ख़ासकर बर्फबारी का मौसम जब लगातार कई दिनों तक आप सिर्फ अपने घर की खिड़कियों से बाहर झांकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कभी बादलों से ज़र्द आसमान में नीली पौ फटने की आस लिए ताकते और कभी ज़मीन में कितने इंच बर्फ जमी है, इसका अंदाज़ा लगाते हुए।
एक वक्त था जब आबादी और विकास के करीब माने जाने वाले इलाकों में भी बर्फ के बाद कम अज़ कम महीने भर के लिए बिजली का गुल होना तय होता था। ज़्यादा ऊंची जगहों पर ये अवधि 4-5 महीने तक होती थी। बिजली के खंभे इतने मज़बूत हो ही नहीं पाते थे कि एक सीज़न की बर्फबारी झेल पाएं। इन दिनों में छह-सात बजे ही रात का खाना मजबूरी ही होती थी। इसके बाद चूल्हे की आंच तापते हुए गपशप ही मनोरंजन का इकलौता ज़रिया हुआ करती थी। लेकिन क्या मनोरंजन होता था वो!

ऐसी ही दोपहरों और शामों में बर्फ से सफेद मंज़र की नि:शब्दता को बाहर पंछियों के झुंड़ों की हलचल तोड़ती थी और घर की रसोई में चूल्हे की आग तापते दादाजी की तिलिस्म से भरी हुई कहानियां। वे अक्सर घर के बाकी लोगों के सो जाने के बाद भी वहीं बैठे गुनगुनाया करते थे। जब तक कि लकड़ियों से कुरेदने के बाद राख़ में सेंकने लायक अंगार बाकी हों।
मेरे जो दोस्त पहाड़ से हैं वो इस ‘नॉस्टेलजिया’ को शायद इसलिए ना समझें क्योंकि वो इस अनुभव के बेहद करीब हैं और जो पहाड़ से नहीं हैं उन्होंने इसे कभी जिया नहीं। लेकिन मैं इन स्मृतियों को छोड़ना नहीं चाहता। मोह ही कह लीजिए। अच्छी बात ये है कि हमारे यहां अब भी बहुत सारी चीज़ों पर आधुनिकता का रोगन नहीं चढ़ पाया है। कुछ मामलों में परंपराओं के टूटने का भय और कुछ मामलों में ज़रूरत का तकाज़ा।

संपन्न घरों में आपको डिजाइनर किचन मिल जाएंगे लेकिन चूल्हे की एक अलग रसोई भी होगी। उज्ज्वला जैसी योजनाओं से काफी पहले ही ज़्यादातर रसोई घरों में गैस सिलिंडर पहुंच चुके थे लेकिन चूल्हे टूटे नहीं। टूटने भी नहीं चाहिएं। घर के चार लोग बैठे तो एक ही कमरे में हों लेकिन एक साथ नहीं बल्कि चार अलग-अलग मोबाइल फोन के साथ। चूल्हे ये सुनिश्चित करने का एक ज़रिया हैं कि ऐसे दुर्दिन हमारे गांवों को कभी ना देखने पड़ें। आमीन।
(लेखक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से हैं और विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक विषयों पर लिखते रहते हैं।)